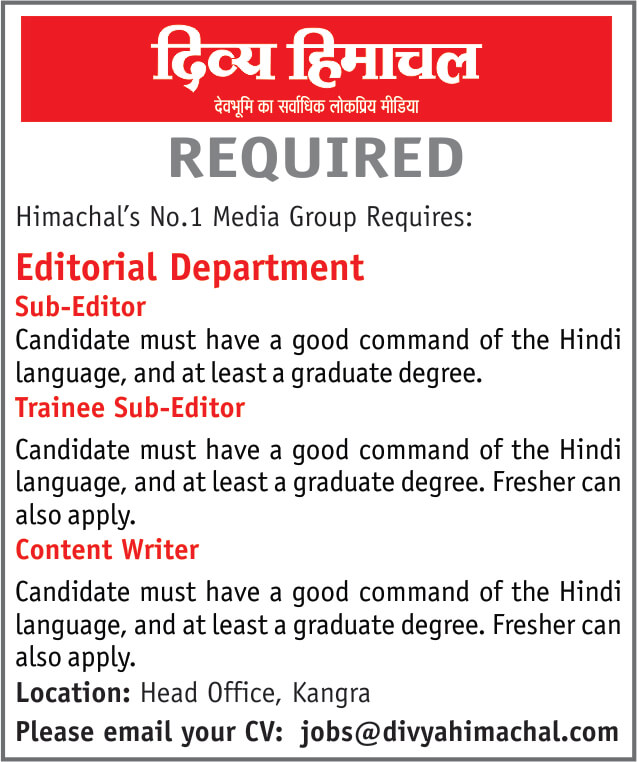देशी उत्पादों को खरीदे सरकार

अभी तक सरकारी खरीद में भी आयातित विदेशी वस्तुओं की भरमार रहती है। उसके कई कारण हैं। सरकार में प्रतिस्पर्धी निविदाओं के आधार पर खरीद होती है। ऐसे में सस्ते चीनी उत्पाद उपलब्ध होते हैं, वहां उन्हीं वस्तुओं की खरीद हो जाती है। माना जाता है कि कम से कम दो खरब रुपए की खरीद सरकार द्वारा होती है। ऐसे में देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की तमाम कोशिशों को बड़ा धक्का लगता है। इसलिए जरूरी है कि देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में बनी वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता मिले…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता के सूत्र संभालने के बाद, अपनी आर्थिक नीति के जिन प्रमुख बिंदुओं की घोषणा की, उसमें मेक इन इंडिया प्रमुख था। गौरतलब है कि 2007-08 में जहां हमारे औद्योगिक उत्पादन की ग्रोथ की दर, जो 15 प्रतिशत से ज्यादा थी, 2011-12 के बाद के वर्षों में शून्य और कभी-कभी ऋणात्मक हो चुकी थी। यानी औद्योगिक विकास थम सा चुका था। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर ही नहीं, छोटी-बड़ी उपभोक्ता वस्तुओं, फर्नीचर आदि सब कुछ चीन या अन्य देशों से आने लगा था। देश में कोई नई फैक्टरी नहीं लग रही थी और पहले चल रही फैक्टरियां भी चीन में शिफ्ट होने लगीं। जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा मात्र 15 प्रतिशत के आसपास बना रहा। ऐसे में मई, 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि नीतियों की घोषणा हुई। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कहा कि उनकी नीति भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की है। उसमें उन्होंने यह कहा कि वह दुनिया भर की कंपनियों से अपील करते हैं कि वे आएं और भारत में उत्पादन करना शुरू करें। उधर सरकार ने भारत के उद्यमियों से कहा कि वे देश में उद्योग लगाए और उन्हें विभिन्न कठिनाइयों से निजात दिलाई जाएगी। ‘ईज ऑफ डूइंग’ बिजनेस को भी बेहतर किया जाएगा। युवा उद्यमियों को जो नए उद्यम यानी स्टार्टअप लगाएंगे, उनके लिए बिजनेस की सुविधा, करों में छूट और सहयोग सभी उपलब्ध कराने की बात की गई। पहली बार व्यवसाय बढ़ाने हेतु इतने बड़े स्तर पर प्रयास हुआ। स्टार्टअप, स्टैंडअप, होल्डिंग हैंड आदि नए शब्द सरकारी शब्दकोष में जुड़ गए। हालांकि इन सब प्रयासों का परिणाम आने में समय लग सकता है, लेकिन यह भी सही है कि औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास को लेकर वातावरण में कुछ बेहतरी जरूर हुई है। नए स्टार्टअप खुलने शुरू हुए हैं और सरकार का रवैया भी ‘होल्डिंग हैंड’ वाला है। जहां औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की पहली शर्त उद्योगों की स्थापना तो है ही, इसके लिए जरूरी है कि देश में उन वस्तुओं की मांग भी हो।
दुर्भाग्य से पिछले काफी समय से औद्योगिक वस्तुओं, चाहे वे उपभोक्ता वस्तुएं हों या मशीनरी सरीखी उत्पादक वस्तुएं, का आयात बढ़ता जा रहा था। उसकी तुलना में निर्यात बहुत कम थे। इसका मतलब यह है कि हमारे यहां औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और उसे अपने ही देश में खपाने की बहुत संभावनाएं हैं। 1995 से आस्तित्व में आए डब्ल्यूटीओ समझौतों के अनुसार सभी सदस्य देशों द्वारा आयात शुल्क (टैरिफ) को शून्य या उसके आसपास रखने की प्रतिबद्धता निश्चित की गई थी। यही नहीं, आयातों को रोकने के गैर-टैरिफ तरीकों यानी गैर टैरिफ बाधाओं को भी समाप्त करने की प्रतिबद्धता ली गई। सस्ते श्रम, सरकारी सबसिडी और कई अनैतिक तरीकों के कारण चीन का माल सस्ता होने की वजह से दुनिया भर दुनिया के बाजारों में छाने लगा। यह इस बात से पता चलता है कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2015-16 में 52.7 अरब डालर तक पहुंच गया। दुनिया भर में चीन का व्यापार सरप्लस 2016 में 486 अरब डालर तक पहुंच चुका था। अभी तक सरकारी खरीद में भी आयातित विदेशी वस्तुओं की भरमार रहती है। उसके कई कारण हैं। सरकार में प्रतिस्पर्द्धी निविदाओं के आधार पर खरीद होती है। ऐसे में सस्ते चीनी उत्पाद उपलब्ध होते हैं, वहां उन्हीं वस्तुओं की खरीद हो जाती है। माना जाता है कि कम से कम दो खरब (दो लाख करोड़) रुपए की खरीद सरकार द्वारा होती है। ऐसे में देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की तमाम कोशिशों को बड़ा धक्का लगता है। इसलिए जरूरी है कि देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में बनी वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता मिले। नई आर्थिक नीति लागू होने से पहले भी लघु उद्यागों/खादी उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन नई आर्थिक नीति के लागू होने बाद इस प्राथमिकता को बदला गया। पहले तो खरीद में प्राथमिकता को बदल कर कीमत प्राथमिकता में बदला गया और बाद में धीरे-धीरे कर इस प्राथमिकता को भी समाप्त कर दिया गया। डब्ल्यूटीओ समझौतों के बाद यह भी तर्क दिया जाता रहा है कि चूंकि हमें विदेशी कंपनियों/आयातों को भारतीय उत्पादों के समान व्यवहार देना बाध्यकारी है, इसलिए हम उनकी तुलना में भारतीय और यहां तक कि लघु उद्योगों के भी सामान को प्राथमिकता नहीं दे सकते। अमरीकी सरकार ‘बाई अमेरिकन एक्ट 1933’, के अंतर्गत सरकारी खरीद में अमरीका के बने उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है। डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुसार यदि सरकार अपने स्वयं के उपभोग के लिए उस देश के बने उत्पादों को प्राथमिकता दे, तो यह नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन किसी कंपनी द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए देश में बने समान को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वह डब्ल्यूटीओ का उल्लंघन माना जाएगा।
इसलिए जब सरकार ने जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन में स्वदेशी उत्पादों की खरीद की शर्त रखी, तो उसे डब्ल्यूटीओ द्वारा खारिज कर दिया गया था। चूंकि यह स्पष्ट है कि सरकार स्वयं की आवश्यकता के लिए यदि देश में बने उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देती है, तो इसमें डब्ल्यूटीओ के समझौतों का उल्लंघन नहीं होता। सोलर मिशन में जब अमरीका ने भारत द्वारा स्थानीय सौर उपकरणों के उपयोग की शर्त के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में विवाद खड़ा किया तो भारत इस कारण से उस विवाद में हार गया, क्योंकि सौर ऊर्जा विकास में लगी कंपनियों द्वारा सौर ऊर्जा की व्यावसायिक बिक्री की जानी थी। लेकिन जब अमरीका स्वयं सरकारी खरीद में अमरीकी वस्तुओं को प्राथमिकता देता है, तो भारत के खिलाफ ऐसा मुकदमा नहीं चल सकता। मंत्रालयों के सचिवों की एक समिति द्वारा ऐसी सिफारिश प्रधानमंत्री को की गई है कि ‘मेक इन इंडिया’ नीति को सफल करने के लिए सरकारी खरीद में देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता दी जाए। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जल्दी ही ऐसी नीति को हरी झंडी दे देगी और वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में नियमों को जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि आज थाइलैंड और चीन से भारी मात्रा में उत्पाद आयात किए जा रहे हैं, जिन्हें सरकारी खरीद में शामिल किया जाता है। माना जा सकता है कि देश में बने उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने से देश में ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम वास्तव में सफल हो पाएगा। औद्योगिक जगत भी इस प्रकार के नीतिगत प्रस्ताव से प्रसन्न दिखाई देता है, क्योंकि इससे उसे अपने सामान के लिए एक आश्वस्त बाजार मिलने वाला है।
ई-मेल : ashwanimahajan@rediffmail.com
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App