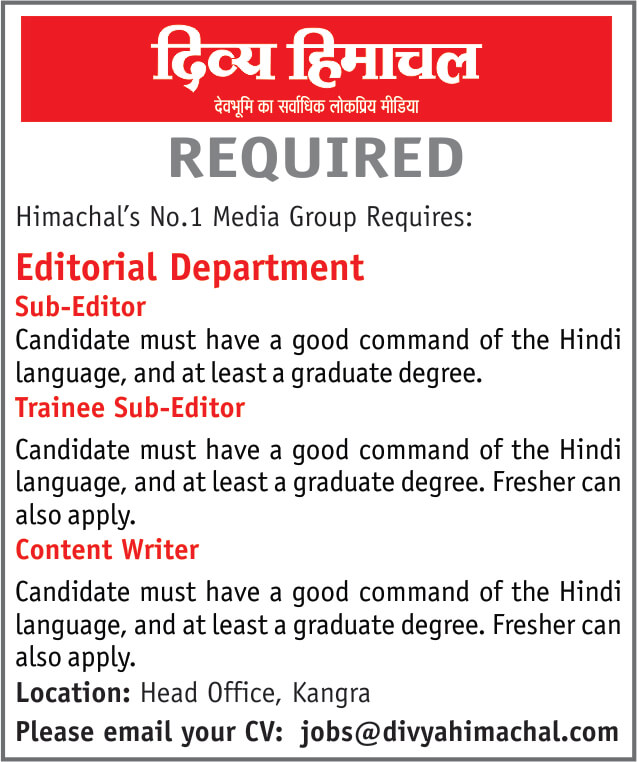उथली व्याख्याओं का चुनाव
लेखक, वरिष्ठ स्तंभकार हैं

भारत के चौदहवें राष्ट्रपति बनने के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के रामनाथ कोविंद और बिहार से मीरा कुमार। रामनाथ अभी हाल तक बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। दूसरी प्रत्याशी मीरा कुमार, स्वर्गीय जनजीवन कुमार की पुत्री हैं। जनजीवन राम कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे और वे लंबे अरसे तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे। लेकिन उन्होंने 1977 में अपने कुछ साथियों सहित कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने मुड़ कर कांग्रेस की ओर नहीं देखा। मीरा कुमार उन्हीं जनजीवन राम की विरासत को संभाले हुए हैं। दोनों प्रत्याशी देश भर में जाकर विधानसभाओं के सदस्यों से वोट देने का अनुरोध कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद का समर्थन भाजपा व उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी उनको समर्थन कर रहे हैं, जिनकी गणना भाजपा के सहयोगी दलों में नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू का इस लिहाज से विशेष उल्लेख किया जा सकता है। मीरा कुमार कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। लेकिन सीपीएम ने अपना प्रत्याशी न खड़ा कर कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करने का ही निर्णय किया है। धीरे-धीरे कांग्रेस के नजदीक खिसकते जाने का कारण शायद सीपीएम में हो रहे वैचारिक परिवर्तन का परिणाम हो। मीरा कुमार के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है।
इसी प्रकार रामनाथ कोविंद के पास उच्चतम न्यायालय में वकालत करने का लंबा अनुभव है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए थे, लेकिन सामाजिक कार्यों में रुचि होने के कारण उन्होंने नौकरी करने के बजाय वकालत को अधिमान दिया। बारह साल तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे। गांव में अपनी पैतृक संपत्ति उन्होंने सामाजिक जन कल्याण के लिए भेंट कर दी। उनके पास कोई पैतृक राजनीतिक विरासत नहीं है, लेकिन वह अपने परिश्रम और योग्यता के बलबूते इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहना होगा कि राष्ट्रपति पद के इन दोनों उम्मीदवारों के विश्लेषण में देश का मीडिया उनके दलित होने को ही अधिमान दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी यही चर्चा हो रही है। मानों उनका दलित समाज से होना ही उनका सबसे बड़ा गुण है। अंग्रेजों के चले जाने के सत्तर साल बाद भी हम जाति की इस मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए गुण प्रमुख होगा या जाति? कबीर ने अरसा पहले कहा था -जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। लेकिन आज भी म्यान पर ही चर्चा हो रही है, तलवार की ओर कोई झांक कर भी नहीं देखता। बीसवीं शताब्दी में सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ताकि जाति गौण हो जाए और व्यक्ति प्रमुख हो जाए। जाति की छाया में छिपा हुआ व्यक्ति बाहर निकल आए, ताकि भारतीय अथवा हिंदू समाज समरस हो सके। इस सामाजिक क्रांति के चार स्तंभ माने जाते हैं। महात्मा गांधी, डा. केशव राव बलीराम हैडगेवार, राम मनोहर लोहिया और भीमराव रामजी अंबेडकर। इनके प्रयासों से भारतीय अथवा हिंदू समाज में निरंतर सागर मंथन हुआ और यह प्रक्रिया किसी सीमा तक अभी भी चली हुई है। यह इसी सागर मंथन का परिणाम था कि दलित समाज के लोग सत्ता शिखरों तक पहुंचे।
इतना ही नहीं, हिंदू समाज में व्यापक स्तर पर उनके इस आरोहण को एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर ही देखा गया। जहां समाज में शताब्दियों से जाति के आधार पर इतनी विषमता रही हो कि एक बड़ा वर्ग अस्पृश्य ही मान लिया गया हो, वहां दलित आरोहण की ये घटनाएं सामान्य मान ली गईं। यह भारतीय समाज की आंतरिक एकता का परिचायक है, जिसे विदेशी विद्वान कभी समझ नहीं पाएंगे। यह बात भीमराव अंबेडकर ने 1912 में अमरीका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपना जाति विषयक निबंध प्रस्तुत करते हुए कही थी। उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था को लेकर विदेशी विद्वानों के तमाम विश्लेषणों को नकारा था और जातियों के बावजूद भारत की सांस्कृतिक एकता के आंतरिक सूत्रों की चर्चा की थी। लगता है कि 1912 में भीमराव अंबेडकर के अकाट्य तर्कों को सुन कर विदेशी विद्वानों ने तो भारतीय मन को न समझ पाने की अपनी असमर्थता को स्वीकार कर लिया था, परंतु भारत का अंग्रेजी भाषा का मीडिया अपनी इस असमर्थता को अभी भी स्वीकार कर लेने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार का नाम आते ही यह मीडिया उनके दलित होने को ही महिमामंडित करने के काम में जुट गया। भारतीय समाज केवल जाति के खांचों में ही नहीं बंटा हुआ। वह जाति से ऊपर उठ कर भी कार्य करता है। जाति उसके सामाजिक जीवन का एक अंश हो सकती है, वह संपूर्ण अंश नहीं है। यदि ऐसा न होता, तो भाजपा उत्तर प्रदेश के चुनाव इतने प्रचंड बहुमत से न जीत पाती। हिंदू समाज ने अपनी इस भीतरी सांस्कृतिक सामाजिक एकता का प्रदर्शन एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार किया है। लेकिन लगता है कि अंग्रेजी मीडिया राजा जनक के उन दरबारियों की तरह काम कर रहा है, जो अष्टावक्र को देखते ही अट्टहास करने लगे थे। लेकिन अंत में उन्हें स्वयं अपमानित होना पड़ा था। ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति देश के 125 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी जाति विशेष का। ताज्जुब तो इस बात का है कि देश की आम जनता में तो बहस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को लेकर हो रही है, लेकिन देश के विदेशी भाषाओं मसलन अंग्रेजी, फ्रेंच और पुर्तगाली के मीडिया में बहस उम्मीदवारों की जाति को लेकर हो रही है। अब इस चुनाव में उभर रहे कुछ प्रमुख मुद्दों की बात कर ली जाए।
रामनाथ कोविंद के पक्ष में देश के लगभग अधिकांश राजनीतिक दल एकत्रित हो गए हैं। इसका एक प्रमुख कारण उनका अब तक का बेदाग व्यक्तित्व है। शुरू में यह भी लगता था कि कांग्रेस शायद अपना उम्मीदवार ही न खड़ा करे। लेकिन बाद में शायद कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक विवशता के चलते मीरा कुमार को मैदान में उतारा। इसी से हैरान होकर शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख प्रकट किया कि जब हारने की बारी आई, तो कांग्रेस ने उसके लिए बिहार की बेटी का चयन क्यों किया। जिन दिनों कांग्रेस राष्ट्रपति का चुनाव जीतने की स्थिति में थी, तब उन्हें मीरा कुमार का ध्यान क्यों नहीं आया? लगता है कि मीरा कुमार भी इसको अच्छी तरह जानती हैं कि वह अपनी पार्टी की राजनीति की शतरंज पर मोहरा बन गई हैं। शायद इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के मतदाताओं से अपील की है कि वे वोट अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन कर दें। राष्ट्रपति चुनाव के दंगल में यह अपील सबसे पहले इंदिरा गांधी ने की थी। वह कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखती थीं। पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ा किया था। एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरि भी चुनाव मैदान में उतर आए थे। इंदिरा गांधी कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव अभियान में उतरीं, तो उन्होंने मतदाताओं से अपील कि कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन कर वोट दें। उस समय इसका यह अर्थ निकाला गया था कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मतदाता, इस बात की चिंता मत करें कि कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी कौन है, बल्कि वे वोट देते समय अपनी आत्मा की आवाज सुनें और उसी के अनुसार वोट दें। सचमुच ही कांग्रेस के मतदाताओं ने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। अब वही जुमला 2017 में कांग्रेस की प्रत्याशी मीरा कुमार दोहरा रही हैं। राजनीतिक हलकों में इसके दोहरे अर्थ निकाले जा रहे हैं। क्या वह भी इंदिरा गांधी की तरह कांग्रेस पार्टी के मतदाताओं को संबोधित कर रही हैं?
ई-मेल : kuldeepagnihotri@gmail.com
भारत मैट्रीमोनी पर अपना सही संगी चुनें – निःशुल्क रजिस्टर करें !
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App