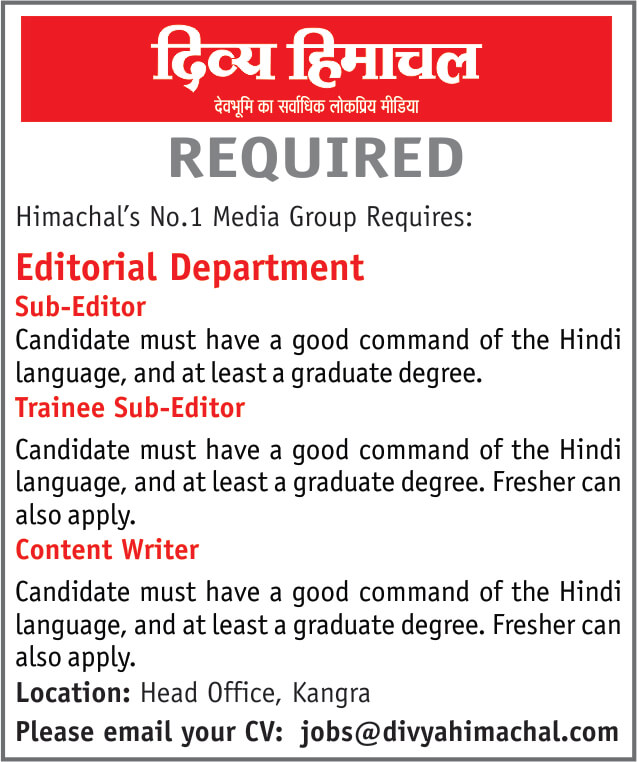ईश्वर की खोज
स्वामी विवेकानंद
गतांक से आगे… ईश्वर की भक्ति प्रत्येक धर्म में दिखाई देती है, वह दो भागों में विभाजित होती है। वह जो रूपों और अनुष्ठानों और शब्दों द्वारा कार्य करता है और वह जो प्रेम द्वारा कार्य करती है। इस संसार में हम नियमों से बंधे हैं और सदा उन्हें तोड़कर निकल जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, हम सदा नियमों का उल्लंघन, प्रकृति को कुचलने का प्रयत्न करते रहते हैं। उदाहरण के लिए प्रकृति हमें घर नहीं देती, हम उन्हें बनाते हैं। प्रकृति ने हमें नग्न बनाया है, हम अपने को वस्त्रों से ढंकते हैं। मनुष्य का लक्ष्य मुक्त होना है और बस, जहां तक हम प्रकृति के नियमों को तोड़ने में असफल रहते हैं, वहीं तक उन्हें सहन करते हैं। हम प्रकृति के नियमों का पालन इसलिए करते हैं कि नियमों से परे, नियमों से बाहर निकल जाएं। जीवन का समस्त संघर्ष नियम न मानना है। (इसीलिए मैं, ईसाई वैज्ञानिकों से सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि वे मनुष्य की स्वतंत्रता और आत्मा के दिव्यत्व की शिक्षा देते हैं)। आत्मा सब परिस्थितियों से ऊपर है। ‘ब्रह्मांड मेरे पिता का राज्य है, मैं उसका उत्तराधिकारी हूं’ मनुष्य को यह भाव अपनाना चाहिए। ‘मेरी आत्मा सब वशीभूत कर सकती है।’ मुक्ति तक पहुंचने से पहले हमें नियम से कार्य करना होगा। बाहरी सहायताएं और विधियां, रूप, अनुष्ठान, विश्वास, सिद्धांत सबका अपना समुचित स्थान है और उनका उद्देश्य उस समय तक हमें सहारा देना और शक्ति प्रदान करना है, जब तक कि हम सशक्त न हो जाएं। इसके बाद वे आवश्यक नहीं रह जातीं। वे हमारी धाय हैं और इस रूप में बचपन में अनिवार्य हैं। पुस्तकें भी धाय हैं, औषधियां धाय हैं। पर हमें वह समय लाने के लिए काम करना होगा, जब मनुष्य स्वयं अपने शरीर पर अपने स्वामित्व को पहचानने लगेगा। जड़ी-बूटियां और औषधियां हमारे शरीर पर उसी समय तक प्रभाव डालती हैं, जब तक हम उन्हें ऐसा करने देते हैं। जब हम सबल हो जाते हैं, तो बाहरी विधियों की आवश्यकता नहीं रहती। शब्दों द्वारा भक्ति शरीर मन का ही स्थूलतर रूप है, मन सूक्ष्मतर स्तरों से बना हुआ है और शरीर स्थूलतर स्तरों से और जब मनुष्य का मन पूर्णतया उसके वश में आ जाता है, तो उसका शरीर भी उसके वश में आ जाता है। जिस प्रकार प्रत्येक मन का अपना विशिष्ट शरीर होता है, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द एक विशिष्ट विचार का अंग होता है। जब हम क्रुद्ध होते हैं, तो पुरुष व्यंजनों में बोलते हैं-‘बुद्धू’, ‘मूर्ख’, ‘गधा’ आदि जब हम करुण होते हैं, तो कोमल स्वरों का उपयोग करते हैं ‘अरे राम!’ निश्चय ही ये क्षणिक भाव है, पर चिरंतन भाव भी होते हैं, जैसे प्रेम, शांति, स्थिरता, आनंद, पवित्रता और सब धर्मों में इन भावों की शब्दाभिव्यक्ति हुई है, शब्द मनुष्य के इन उच्चतम भावों के केवल शरीर हैं। विचार शब्द उत्पन्न करता है और अपनी बारी आने पर शब्द विचार अथवा भाव उत्पन्न कर सकते हैं। यहीं शब्दों की सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रत्येक शब्द एक आदर्श का द्योतन करता है। हम सब इन पवित्र और रहस्मयी शब्दों को पहचानते और जानते हैं, किंतु यदि हम उन्हें केवल पुस्तकों में पड़ते हैं, तो वे हमें प्रभावित नहीं करते।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App