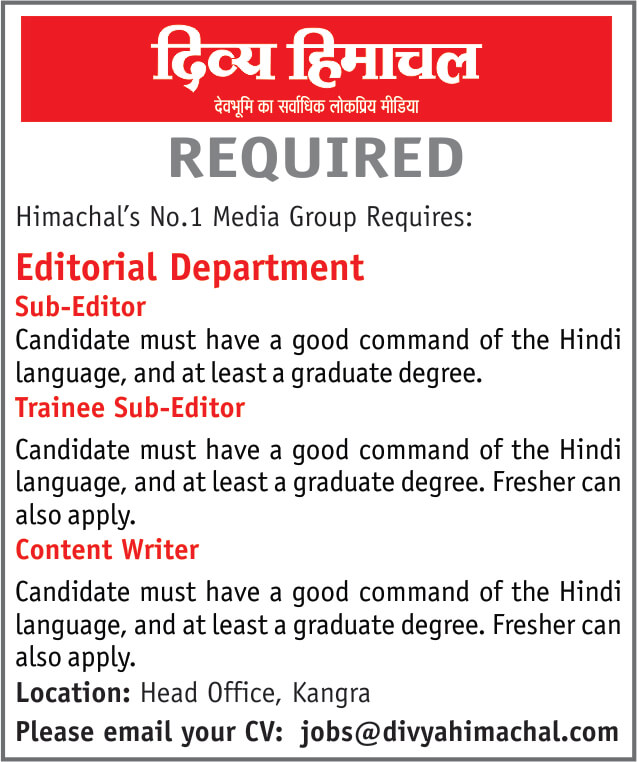हिमाचली हिंदी कहानी : विकास यात्रा : 57

कहानी के प्रभाव क्षेत्र में उभरा हिमाचली सृजन, अब अपनी प्रासंगिकता और पुरुषार्थ के साथ परिवेश का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। गद्य साहित्य के गंतव्य को छूते संदर्भों में हिमाचल के घटनाक्रम, जीवन शैली, सामाजिक विडंबनाओं, चीखते पहाड़ों का दर्द, विस्थापन की पीड़ा और आर्थिक अपराधों को समेटती कहानी की कथावस्तु, चरित्र चित्रण, भाषा शैली व उद्देश्यों की समीक्षा करती यह शृंखला। कहानी का यह संसार कल्पना-परिकल्पना और यथार्थ की मिट्टी को विविध सांचों में कितना ढाल पाया। कहानी की यात्रा के मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक पहलुओं पर एक विस्तृत दृष्टि डाल रहे हैं वरिष्ठ समीक्षक एवं मर्मज्ञ साहित्यकार डा. हेमराज कौशिक, आरंभिक विवेचन के साथ किस्त-57
हिमाचल का कहानी संसार
विमर्श के बिंदु
1. हिमाचल की कहानी यात्रा
2. कहानीकारों का विश्लेषण
3. कहानी की जगह, जिरह और परिवेश
4. राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचली कहानी की गूंज
5. हिमाचल के आलोचना पक्ष में कहानी
6. हिमाचल के कहानीकारों का बौद्धिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक व राजनीतिक पक्ष
लेखक का परिचय
नाम : डॉ. हेमराज कौशिक, जन्म : 9 दिसम्बर 1949 को जिला सोलन के अंतर्गत अर्की तहसील के बातल गांव में। पिता का नाम : श्री जयानंद कौशिक, माता का नाम : श्रीमती चिन्तामणि कौशिक, शिक्षा : एमए, एमएड, एम. फिल, पीएचडी (हिन्दी), व्यवसाय : हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में सैंतीस वर्षों तक हिन्दी प्राध्यापक का कार्य करते हुए प्रधानाचार्य के रूप में सेवानिवृत्त। कुल प्रकाशित पुस्तकें : 17, मुख्य पुस्तकें : अमृतलाल नागर के उपन्यास, मूल्य और हिंदी उपन्यास, कथा की दुनिया : एक प्रत्यवलोकन, साहित्य सेवी राजनेता शांता कुमार, साहित्य के आस्वाद, क्रांतिकारी साहित्यकार यशपाल और कथा समय की गतिशीलता। पुरस्कार एवं सम्मान : 1. वर्ष 1991 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भारत के राष्ट्रपति द्वारा अलंकृत, 2. हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी की सतत उत्कृष्ट एवं समर्पित सेवा के लिए सरस्वती सम्मान से 1998 में राष्ट्रभाषा सम्मेलन में अलंकृत, 3. आथर्ज गिल्ड ऑफ हिमाचल (पंजी.) द्वारा साहित्य सृजन में योगदान के लिए 2011 का लेखक सम्मान, भुट्टी वीवर्ज कोआप्रेटिव सोसाइटी लिमिटिड द्वारा वर्ष 2018 के वेदराम राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत, कला, भाषा, संस्कृति और समाज के लिए समर्पित संस्था नवल प्रयास द्वारा धर्म प्रकाश साहित्य रतन सम्मान 2018 से अलंकृत, मानव कल्याण समिति अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा साहित्य के लिए अनन्य योगदान के लिए सम्मान, प्रगतिशील साहित्यिक पत्रिका इरावती के द्वितीय इरावती 2018 के सम्मान से अलंकृत, पल्लव काव्य मंच, रामपुर, उत्तर प्रदेश का वर्ष 2019 के लिए ‘डॉ. रामविलास शर्मा’ राष्ट्रीय सम्मान, दिव्य हिमाचल के प्रतिष्ठित सम्मान ‘हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड’ ‘सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार’ सम्मान 2019-2020 के लिए अलंकृत और हिमाचल प्रदेश सिरमौर कला संगम द्वारा डॉ. परमार पुरस्कार।
डा. हेमराज कौशिक
अतिथि संपादक
मो.-9418010646
-(पिछले अंक का शेष भाग)
गंगाराम राजी के ‘उल्लू न बनाओ’ शीर्षक कहानी संग्रह में सोलह कहानियां- बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, पीं पीं खुशी, सन्नाटा, जब मैं आया अपने गांव, लाल बत्ती, चल उड़ जा रे पंछी, उल्लू न बनाओ, ऑपरेशन, जोरावरी, आके ढ़ाके पासो दे झाटे, ऐसा भी होता है, डण्डा पीर, पुरानी नायिका का मिलना, चाय फिर झाड़ू, अब सडक़ वाला जीएम, नकली चूहिया, ऋण नहीं उतार पाऊंगा और पटाक्षेप संगृहीत हैं। ‘उल्लू न बनाओ’ प्रस्तुत कहानी संग्रह की शीर्षक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली के संदर्भ में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का चित्रण किया है। कहानीकार ने यह स्थापित किया है कि इसके लिए स्वयं रिश्वत देने वाला भी पर्याप्त सीमा तक जिम्मेदार है। ‘लाल बत्ती’ शीर्षक कहानी मुंबई जैसे महानगरों में भिक्षावृत्ति करने वाले वर्ग की कहानी प्रस्तुत करती है। मुंबई के चौराहे पर लाल बत्ती जलने पर गाडिय़ों के रुकने पर भिखारियों की भीड़ में वृद्ध, जवान युवक युवतियां, बालक, बालिकाएं भिक्षा की याचना के लिए हाथ बढ़ाते हैं। उन्हीं में से यौवन की दहलीज पर पहुंची युवतियों को पैसे का लालच देकर कार में बलपूर्वक उठा कर ले जाते हैं और उन्हें वासना का शिकार बनातें हैं। ‘ऑपरेशन’ शीर्षक कहानी में एक लेखक के प्रति उसके परिवार के सदस्यों का उसकी कृतियों के प्रति उपेक्षा भाव को प्रकाशक द्वारा भेजे गए पुस्तकों के पार्सल के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। पार्सल को देखकर पुत्रवधू में उल्लास और जिज्ञासा उत्पन्न होती है, परंतु पार्सल को खोलने पर पुस्तकों को देखकर नाक भौं सिकुडऩे की मुद्रा इसकी परिचायक होती है।
लेखक की नई पुस्तक के प्रति उनमें किसी प्रकार का उल्लास उत्पन्न नहीं होता। परंतु पौत्र को दादू का फोटो देखकर उल्लास होता है। लेखक सोचता है कि बड़ा होकर वह भी ऐसा ही हो जाएगा। ‘बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए’ निम्न मध्यवर्गीय परिवार की पति-पत्नी की रूढि़वादी सोच से उत्पन्न दस संतानों के भरे पूरे परिवार के पालन पोषण की कठिनाइयों, ढाबा चलाने पर पति-पत्नी की दुर्बलताओं और शौक, आर्थिक कठिनाइयों से जूझने की स्थितियों, संगीत सुनने की रुचि आदि से संबद्ध अनेक कथा सूत्र कहानी में विन्यस्त किए गए हैं। ‘पुरानी नायिका का मिलना’ में प्रेम के अंतद्र्वंद्व को रुखसाना के संदर्भ में निरूपित किया है। यह एक मार्मिक कहानी है। ‘पांच बीघा जमीन’ शीर्षक कहानी संग्रह में बारह कहानियां- सरकार बनाम आदमी, आई लव यू पापा, रिश्ते कैसे बनते हैं, तब अब और आगे, पेंशन है तो टैंशन नहीं, पांच बीघा जमीन, हरा समुंद्र गोपी चंद्र, सुसाइड नोट, चाय फिर झाड़ू, अब सडक़ वाला जीएम, खेसड़ी और एकलव्य संगृहीत हैं। ‘सरकार बनाम आदमी’ शीर्षक कहानी में कहानीकार ने मुरारी की चरित्र सृष्टि के माध्यम से युवा पीढ़ी की हताशा, निराशा, पढ़ लिखकर आजीविका के साधन उपलब्ध न होने पर आत्महत्या करने की कोशिश पर पुलिस द्वारा पकडऩे पर सजा देने और न मरने देने का चित्रण है। मुरारी पढ़ा लिखा युवक है। एमए तक शिक्षा अर्जित की है, परंतु बेकारी में भटकता है। कहानी युवा वर्ग की दिग्भ्रमित होने की स्थितियों का निरूपण करती है। ‘पांच बीघा जमीन’ शीर्षक कहानी में रेशमु-त्वारसु दंपति को भूमिहीन होने के कारण पांच बीघा जमीन मिलने की कहानी है। प्रधान, पटवारी, पंडित सभी उसकी जमीन पर लुब्ध दृष्टि रखते हैं और उसका शोषण करते हैं। ‘आई लव यू पापा’ कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है जिसमें बालकों की रचनात्मकता और उनके प्रति अभिभावकों के निषेधात्मक दृष्टिकोण को सामने लाया है। ‘एक भीगी सुबह’ में दस कहानियां- लॉलीपॉप के चक्कर में, दर्द की दवा क्या है, एक भीगी सुबह, भागते चोर की लंगोटी, हर पल जी भर कर जिओ, सुंदरता वर्सिस असुंदरता, क्या से क्या हो गए हम, बुआ, बहुत कठिन डगर है पनघट की और मैं और मेरे दोस्त संगृहीत हैं। ‘क्या से क्या हो गए हम’ कहानी दो युवकों के संदर्भ में युवा पीढ़ी की प्रतिभा के उपयोग और दुरुपयोग को चित्रित करते हुए यह स्थापित करती है कि पुनीत जैसे प्रतिभाशाली युवकों की प्रतिभा का सदुपयोग जब नहीं किया जाता तब राजनायक उनकी प्रतिभा का दुरुपयोग अपने दलगत स्वार्थ की सिद्धि के लिए करते हैं। ऐसे युवक भ्रष्ट राजनीति की दलदल से निकलना चाहते हुए भी निकल नहीं पाते। ‘बुआ’ शीर्षक कहानी में कहानीकार ने उन सुंदर सुशिक्षित युवतियों की नियति को उभारा है जिनकी उम्र पढऩे लिखने, नौकरी तलाश में और वर चयन में निकल जाती है। विवाह के लिए उपयुक्त वर्ग न मिल पाने के कारण परिवार में अपने भाई की संतानों को पढ़ाते और उनकी देखरेख में गुजार देती हैं।
अपने जीवन को समर्पित करने वाली ऐसी युवतियों को अपने जीवन के उत्तरार्ध में भाई-भाभी की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। ‘बहुत कठिन डगर है पनघट की’ कहानी में कहानीकार ने विद्यालय में शिक्षकों की भूमिका, गुरु शिष्य संबंध, सेवा और कर्तव्यनिष्ठा को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए वर्तमान में शिक्षकों के कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप और मीडिया की घटिया रिपोर्टिंग से शिक्षा की डगर जिन आधारभूत कठिनाइयों से गुजर रही है, उसकी तह तक यह कहानी जाती है। ‘दर्द की दवा क्या है’ कहानी में मां की असामयिक मृत्यु पर शोक सभा के संदर्भ में डॉक्टरों के व्यवसाय में आई गिरावट, कर्तव्यविमुखता, रोगी के उपचार में उपेक्षा भाव आदि का चित्रण है। ‘एक भीगी सुबह’ में रजिया प्रमुख चरित्र है। कहानीकार ने हाशिए के इस चरित्र को एक संवेदनशील, वात्सल्यपूर्ण, करुणासिक्त, मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत, गरिमामय चरित्र के रूप में उभारा है, वह अद्भुत है।
नैरेटर को रजिया एक मंदिर में मिलती है, जहां मदद के लिए कहती है। नैरेटर को उसकी जरूरत के संबंध में जिज्ञासा होती है, वह कहती है कि वह किसी अभिजात्य परिवार में बीस साल से नौकरी करती है। मालकिन की बेटी को जन्म से लेकर उसने वहां रहते हुए पाला है। उसका विवाह है, इसलिए उसको विवाह के अवसर पर वह गिफ्ट देना चाहती है, जो बड़े लोगों की बेटी के अनुकूल हो। बेटी के प्रति प्यार और वात्सल्य के कारण वह ऐसा गिफ्ट देना चाहती है जिसके लिए चाहे उसे उम्र भर नौकरी करनी पड़े। वह कहती है गिफ्ट के लिए उसने पैसे जुटाए हैं, कुछ कमी है। वह मुस्लिम है। वह मंदिर में इसलिए आई है कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में आने वाले भक्तों में ही इनसानियत बची है, इसलिए वह मंदिर में मदद की आशा से आई है। नैरेटर उसे मदद का आश्वासन देता है, परंतु नैरेटर के कई दिनों तक प्रतीक्षा करने पर भी वह नहीं लौटती है। एक दिन वह अचानक आती है और विवाह संपन्न होने की सूचना देता है और यह भी बताती है कि उसे मेम साहिबा ने साड़ी दी है और यह कहती है कि इस साड़ी को मेम साहिबा डालती थीं, महंगी होगी। साहिब जी, जरा सी एक जगह से फटी है, पल्लू के नीचे आ जाती है। हम लोगों को बुरा नहीं लगता, सब चलता है। यह कहानी उस तथाकथित अभिजात्य वर्ग की संवेदनशून्यता, अहंकार, ह्रदय संकीर्णता, कृपणता को यथार्थ के धरातल पर अनावृत करती है और हाशिए के समाज की संवेदनशीलता, करुणासिक्तता और वात्सल्य भाव को निरूपित करती है। गंगाराम राजी के ‘कोने का बुहारा हुआ कूड़ा’ शीर्षक कहानी संग्रह में चौदह कहानियां- तब और अब, बंदर की पूंछ, फिर बचपन याद आया, सुख भरी से दुख भरी, हेमकुंभ, चैन कहां आराम कहां, प्यार की कोई सीमा नहीं, विश्वास, लॉलीपॉप के चक्कर में, पटरी-पटरी जीवन, तितली उड़ गई, भजन में रंजन, धत् तेरे की और कोने का बुहरा हुआ कूड़ा संगृहीत हैं। ‘तब और अब’ कहानी में तीन पीढिय़ों की मानसिकता, हृदय की अनुदारता, मानवीय मूल्यों के ह्रास को चित्रित किया है। पहली पीढ़ी के दादा जी दूसरों को भोजन कराए बिना अन्न नहीं ग्रहण करते थे, वहीं दूसरी पीढ़ी के पिता किसी भूखे व्यक्ति को घर से बिना भोजन कराए नहीं जाने देते थे। वहीं तीसरी पीढ़ी के विधायक जन प्रतिनिधि बनकर, जन कल्याण का दावा करने वाला, घर में आए भूखे व्यक्ति को भोजन देने में समर्थ होते हुए भी भोजन नहीं करना चाहते हैं। पति-पत्नी दोनों में बहस हो जाती है। क्योंकि उन्होंने अपने लिए चार रोटियां बनाई हैं जिन्हें पत्नी किसी अन्य को नहीं देना चाहती।
यह कहानी पति-पत्नी दोनों की अनुदारता, अकर्मण्यता और संवेदनशून्यता को चित्रित करती है। ‘हेमकुंभ’ में राम और भिलनी के वृद्धावस्था में अकेलेपन की नियति का चित्रण है। यह कहानी वृद्धों के प्रति संतान की उत्तरदायित्वहीनता और संवेदनशून्यता को निरूपित करती है। बेटा अमरीका में है, पूरी तरह संवादहीनता है। पिता सत्तर वर्ष की अवस्था तक पहुंच कर एकाकी जीवन यापन करने के लिए अभिशप्त है। जीवन भर कठिनाइयों को झेल कर बेटे को उच्च शिक्षा दिलाते हैं और बाद में बेटा विदेश में ही रच बस जाता है। मां समाचार सुनती है कि भारतीय मूल के एक इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टीवी का यह समाचार मां को अचेत अवस्था तक पहुंचा देता है। पुत्र की चिंता में वह दिनों दिन मरणासन्न अवस्था में पहुंचती है, परंतु बेटा कभी भी उसकी सुध लेने की नहीं सोचता। यह कहानी विदेशों में रह रही संतति की कर्तव्यविमुखता, संवेदनशून्य मानसिकता को चित्रित करती है जो विदेश में जाकर अपनी सुख सुविधाओं में अपने माता-पिता के संघर्ष को विस्मृत कर सुखी जीवन यापन करते हैं। ‘प्यार की कोई सीमा नहीं’ शीर्षक कहानी एक लेखक के पशु पक्षियों के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है जिन्हें पक्षी इस तरह मिलते हैं जैसे बच्चे अपने दादा-दादी, माता-पिता से मिलते हैं, प्यार से उन्हें आगे पीछे पकड़ते हैं। लेखक उनके सान्निध्य में तनाव से मुक्त होता है।
लेखक दस बारह कुत्तों और असंख्य चिडिय़ों की सेवा में अपने आप को तनाव मुक्त और प्रसन्नता अनुभव करता है। ‘तितली उड़ गई’ शीर्षक कहानी में बंजारा परिवारों के जीवन संघर्ष, चलते-फिरते जीवन के कारण चलते-फिरते गांव में उनके सुख-दुख, लड़ाई झगड़े, राग द्वेष और आवश्यकता पडऩे पर एक साथ होने, रिश्ते नाते, एक साथ त्योहार मनाने आदि का चित्रण है। बंजारे स्थान स्थान पर अपने करतब दिखाने के लिए अपने किशोर बालक बालिकाओं को जोखिम में डालते हैं। जवान होती बेटी किसी युवक से प्रेम करने लगती है और भाग जाती है तो बंजारा पिता को अपने कारोबार की चिंता होती है। पिता को बेटी के विवाह की चिंता नहीं है, उसे यह चिंता है कि लडक़ी चली गई तो अकेली बंदरी से भीड़ नहीं जुटाई जा सकती। लडक़ी भीड़ के लिए एक मसला है। लडक़ी बिरादरी के लडक़े के साथ उसी तरह भाग जाती है जिस तरह किसी समय में बंजारा दंपत्ति घर से भागे थे और विवाह के बंधन में बंध गए थे और उस समय मां ने उसे बंदरी दी थी। वे बंदरी को साथ लेकर करतब दिखाने लगे थे। ऐसा ही लडक़ी की मां बंजारा से कहती है, ‘सब रात को हुआ, यह तो होना ही था रे, अपने दिन याद कर, अब तो बच्चों के दिन हैं, काम चलाने के लिए मैंने उसे अपनी बंदरिया दे दी। क्या करती? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था उसे देने के लिए। खाली हाथ उसे कैसे भेजती।’ -(शेष भाग अगले अंक में)
विपाशा ने श्रीलाल शुक्ल को किया याद
साहित्य, संस्कृति एवं कला की द्वैमासिक पत्रिका ‘विपाशा’ का नवंबर 2023-फरवरी 2024 अंक साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल पर केंद्रित है। डा. पंकज ललित इस पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। संपादकीय में जो जानकारी उभर कर सामने आई है, उसके अनुसार श्रीलाल शुक्ल ने एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए हिंदी साहित्य में अपना नाम कमाया और तीखे व्यंग्य भी लिखे। वह एक कहानीकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा बाल साहित्यकार के साथ जाने-माने व्यंग्यकार थे। उनकी कई रचनाएं स्कूल और कालेज के सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं और अनेक शोधार्थियों ने उनके लेखन पर पीएचडी की है। लेख एवं टिप्पणियों की शृंखला में शलवार के बहाने एक सांस्कृतिक चिंतन, वह संसद में जाना चाहता है, निराला के बहाने कुछ साहित्य चर्चा और स्वामी से भी ज्यादा स्वामीभक्त जैसी साहित्यिक सामग्री काफी रोचक है। प्रेम जनमेजय, विजय विशाल और पद्म गुप्त अमिताभ के लेख श्रीलाल शुक्ल तथा अन्य साहित्यिक विषयों पर केंद्रित हैं। लालित्य ललित का संस्मरण भी पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। छुट्टियां, यह घर मेरा नहीं, टी. एम. सिंह की कथा, जीवन का एक सुखी दिन और पहली चूक जैसी कहानियां पाठकों का खूब मनोरंजन करेंगी। उपन्यासों के अंश के तहत सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, बिस्रामपुर का संत, बब्बर सिंह और उनके साथी तथा राग-विराग जैसे उपन्यास पाठकों को चिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। ‘जीवन का एक सुखी दिन’ अनेक तरह की घटनाओं को पिरोकर लिखी गई कहानी है। इसका सार है कि अगर सुबह-सुबह दिन की शुरुआत अच्छे से हो जाए, तो दिन भर परेशान नहीं होना पड़ता, कोई परेशानी नहीं आती, और अगर आती भी है तो उसका समाधान सरलता से हो जाता है। इसी तरह ‘पहली चूक’ नामक कहानी का अंत खेती करने के लिए प्रेरित हुए एक युवक को मिली सीख के साथ होता है। यह एक तरह की व्यंग्य कहानी लगती है, जिसमें युवक यह जानकर हतप्रभ होता है कि खेती करने के लिए जिन उपकरणों, समाधानों की जरूरत होती है, वे सब उस गांव से दूर शहर में उपलब्ध हैं, जहां खेती की जाती है। कहानीकार ने इसमें खेती की जरूरतों को लेकर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है। साथ ही यह कहानी यथार्थवादी भी है। विपाशा के इस अंक में अन्य सामग्री भी पाठक की मानसिक क्षुधा को शांत करती है। -फीचर डेस्क
पुस्तक/पत्रिका समीक्षा : राष्ट्रपति प्रणाली पर नया प्रकाश
कई बार खुद को अचूक साबित करने के अवसर पाने के बावजूद भारत की शासन प्रणाली की बहुस्तरीय विफलता पर देश में निरंतर चिंता भरी आवाजें उठ रही हैं। इन आवाजों को शब्द दे रहे हैं देश के कुछ ऐसे लेखक, जो भारत की शासन प्रणाली की तुलना अन्य राष्ट्रों की प्रणालियों से करने के बाद तर्क सहित विकल्प सुझा रहे हैं। इन्हीं लेखकों में एक हैं जशवंत बी. मेहता, जिनकी पुस्तक ‘रिअप्रेजिंग इंडियन डेमोके्रसी (1947-2023) पार्लियामेंट्री टू प्रेजिडेंशियल,’ आजकल खूब चर्चा में है। पुस्तक का शीर्षक ही इसकी विषयवस्तु की पूर्ण व्याख्या करने में सक्षम है, परंतु यह मात्र आरंभ है अंत नहीं, और यही गुण इसे एक सामान्य पाठन सामग्री की श्रेणी से हटाकर एक संग्रहणीय दस्तावेज के समकक्ष ला खड़ा करता है।
भारत की वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली के कई दोषों के कारण देश के लोगों में इसके प्रति निराशा और असंतोष निरंतर बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप इसके प्रभाव और शुचिता पर प्रश्रचिन्ह खड़े हो रहे हैं। इस स्थिति के उदाहरणों सहित समक्ष रखते हुए लेखक जशवंत मेहता हमारी संसदीय प्रणाली में नेताओं के निरंतर बढ़ते मनमाने दखल को कठघरे में खड़ा करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र की एक विख्यात परिभाषा के उलट हमारे देश में इसकी ‘‘नेताओं का, नेताओं के लिए और नेताओं के द्वारा’’ के रूप में भी व्याख्या की जा सकती है। लेखक पुस्तक में प्रकाश डालते हैं कि हमारे यहां चुनावों की संदिग्ध फंडिंग, राजनीति का अपराधीकरण, नौकरशाहों और नेताओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, विधायिका सदस्यों के विधायी कार्यों पर मेहनत करने के अंतर्निहित प्रावधान का अभाव, मंत्रालयों में मनमाना बदलाव, राज्यों और केंद्र में अस्थायी सरकारें, लोगों का विश्वास जीतने में सक्षम राजनेताओं को सामने लाने की व्यवस्था का अभाव और सभी प्रमुख पार्टियों द्वारा पार्टी हाईकमान की इच्छा अनुरूप उम्मीदवारों का चयन आदि कई कारण हैं, जिनके फलस्वरूप वर्तमान शासन प्रणाली के प्रति जनता का विश्वास डगमगाया है।
ऐसा नहीं है कि लेखक ने मात्र संसदीय शासन प्रणाली की असफलताएं इंगित की हैं, अपितु उन्होंने प्रस्तुक में विकल्प भी विस्तार से तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जापान, आदि का उदाहरण देते हुए यह साबित करने का प्रयास किया है कि इनकी शासन प्रणालियों से सीखते हुए और उनमें कुछ आवश्यक फेरबदल कर भारत में वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रपति प्रणाली अपनाई जाए, तो यह बेहतर शासन स्थापित करने में काफी अधिक सहायक होगी। राष्ट्रपति प्रणाली की विभिन्न विशेषताएं भी लेखक ने सामने रखी हैं। इनमें स्थायित्व, उच्च कोटि के पेशेवरों की कैबिनेट में सीधी तैनाती, विधायिका से कार्यपालिका का पृथ्थकरण और पार्टी सिस्टम पर कम ध्यान, विधानपालिका सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता और विधायी मसलों पर पार्टी व्हिप का अभाव आदि गुण शामिल हैं। इसके साथ ही जशवंत मेहता बताते हैं कि राष्ट्रपति प्रणाली में किस प्रकार हर पदाधिकारी के निर्वाचन में जनता की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। चाहे शहर का मेयर तय करना हो, राज्य का गवर्नर या फिर राष्ट्रपति के रूप में देश का सर्वोच्च कार्यकारी सबके निर्वाचन में वोट के रूप में मतदाता की राय सम्मिलित होती है।
उन्होंने राष्ट्रपति प्रणाली में किसी चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार तय करने संबंधी प्रक्रिया पर भी बखूबी प्रकाश डाला है, जिसके तहत पार्टी आका के बजाय पार्टी के सदस्य यह तय करते हैं कि चाहवानों के बीच में से कौन सबसे उचित प्रत्याशी होगा। इसके उलट, लेखक ने भारतीय व्यवस्था पर भी खुलकर तर्कपूर्ण विमर्श प्रस्तुत किया है। और यह भी कि संसदीय प्रणाली में स्पष्ट बहुमत के अभाव में कैसे एक ईमानदार प्रधानमंत्री असहाय हो जाता है। साथ ही पूर्ण बहुमत के बूते अमरीका के राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तियां पाकर भारत के प्रधानमंत्री किस प्रकार मनमाना शासन करते हैं, यह बताने से भी लेखक चूके नहीं हैं। केडब्ल्यू पब्लिशर्ज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली की ओर से प्रकाशित जशवंत बी. मेहता की यह पुस्तक लगभग तीन सौ पन्नों में समाहित है। विषय वस्तु, शोध आधारित तथ्यों, लेखन शैली और छपाई आदि के आधार पर यह एक संग्रहणीय किताब है, जो मात्र पांच सौ पिचानवे रुपए में पेपर बैक प्रारूप में खरीदी जा सकती है।
-अनिल अग्निहोत्री
पुस्तक: रिअप्रेजिंग इंडियन डेमोक्रेसी (1947-2023) पार्लियामेंट्री टू पे्रजिडेंशियल
लेखक: जशवंत बी. मेहता
प्रकाशक: केडब्ल्यू पब्लिशर्ज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
मूल्य: 595/- (पेपर बैक)
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App